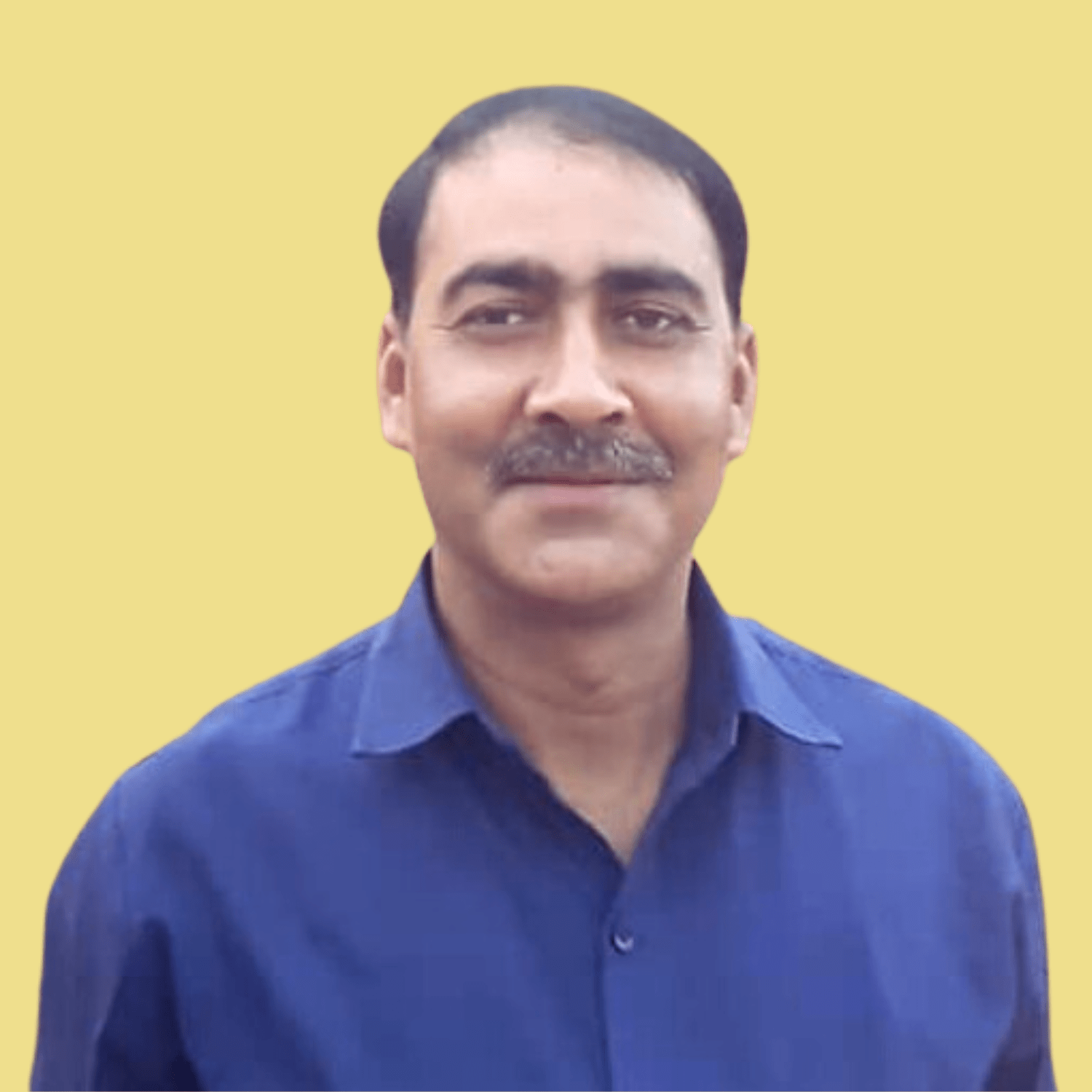
संपर्क- 7697179890, 7974246591
सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का नामांकन, ठहराव और न्यूनतम दक्षता हासिल करना था। अब समग्र शिक्षा का पूरा ध्यान गुणवत्ता पर है। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत स्कूलों में अधिगम का न्यून स्तर, शिक्षकों की कमी और विद्यालय प्रशासन संबंधी कठिनाइयों जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण चुनौती कई छोटे, अकुशल स्कूल चलाना है। छोटे स्कूल पाठशाला ना रहकर भ्रम शाला बन कर रह जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के समान नामांकन के लिए भारत में चीन की तुलना में 5 गुना अधिक स्कूल है तथा भारत के कई राज्यों में 50 फीसद से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 60 से कम छात्रों का नामांकन है। ऐसे में एक अवधारणा स्कूल या पाठशाला विलय की आई। यद्यपि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहलों ने शैक्षिक पहुंच में सुधार किया है। मध्याह्न भोजन योजना छात्र कल्याण का समर्थन करती है तथापि आधे अधूरे संसाधनों और एक शिक्षकीय या शिक्षक विहीन पाठशालाओं ने शिक्षा नीतियों की पोल ही खोली है।
यू डाइस प्लस की 2022 की रपट के अनुसार भारत में कुल 14 लाख 8 हजार 1 सौ पंद्रह विद्यालय हैं जिनमें से सरकारी विद्यालय 10 लाख 22 हजार 3 सौ 86 सरकारी सहायता प्राप्त 82 हजार 4 सौ 80 तथा निजी विद्यालय 34 हजार 7 सौ 53 प्राथमिक पाठशाला 11 लाख 96 हजार 2सौ 65, हाई स्कूल 15 लाख 4 सौ 52 तथा हायर सेकेंडरी 1 लाख 42 हजार 3 सौ 98, एवं इनमें 97 लाख से ज्यादा शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं यू डाइस प्लस की ही 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 26 करोड़ 52 लाख 35 हजार 8 सौ 30 विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पंजीकृत है। यहां यह जानना भी उचित होगा कि साल 2021 में विद्यालयों का आंकड़ा 15 लाख 9 हजार 1 सौ 36 था। इससे साफ पता चलता है कि 1 साल में 1 लाख एक हजार 21 विद्यालय बंद हो गए।2019 में विद्यालयों की संख्या 15 लाख 51 हजार थी। ऐसे समय में नई शिक्षा नीति 2020 से तीन साल पहले ही नीति आयोग ने वर्ष 2017 में “शिक्षण में मानव पूंजी को रूपांतरित करने के लिए सतत कारवाई (सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, साथ-ई) कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसके लिए झारखंड ,ओड़ीसा, एवं मध्यप्रदेश को आदर्श माना गया। झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में कार्यान्वित, साथ-ई परियोजना दक्षता और बेहतर गुणवत्ता के लिए स्कूलों के विलय पर केंद्रित है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसे छह मुद्दों की पहचान की गई है जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बड़े पैमाने पर संबोधित करने की आवश्यकता है जैसे, मजबूत राजनीतिक समर्थन के साथ उप स्तर पर एवं अपर्याप्त संसाधन वाले स्कूलों के मुद्दे को सीधे संबोधित करना, बड़े पैमाने पर शिक्षक रिक्तियों के मुद्दों का समाधान करना, शिक्षक गुणवत्ता एवं शिक्षण शास्त्र में सुधार करना, अधिगम (सीखने) के परिणामो के प्रति जवाबदेही लागू करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और प्रासंगिक मातृभाषा शिक्षा और प्रासंगिक मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान देना, शिक्षा विभागों में शासन संरचनाओं को मजबूत करना अर्थात शिक्षा प्रशासन को मजबूत करना। शिक्षा विलय योजना से शैक्षिक लागत में पर्याप्त बचत हुई, जिसका उदाहरण झारखंड में स्कूल विलय से 2400 करोड़ रुपये की बचत है। 2017 में लॉन्च की गई शिक्षा में मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई (एसएटीएच-ई) परियोजना का उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा को बदलना है। इसमें स्कूलों का विलय, उपचारात्मक कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, भर्ती की निगरानी, जिला और राज्य स्तर पर संस्थानों का पुनर्गठन और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग करना शामिल है। प्रबंधन सूचना प्रणाली, लक्ष्य निर्धारित करने, योजना बनाने, संसाधन आवंटन और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। प्रगति की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संचालन समूह (एनएसजी) और केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) द्वारा की जाती है, और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) द्वारा की जाती है।
नोट: इस लेख को English या अन्य भाषा में पढ़ने के लिए आप सबसे नीचे footer में Change language के माध्यम से भाषा बदल सकते हैं।
स्कूलों के विलय से संसाधन समेकन हो जाता है,जैसा कि 4,380 स्कूलों वाले झारखंड में देखा गया है, महत्वपूर्ण लागत बचत और कुशल संसाधन उपयोग होता है। बड़े स्कूल बेहतर सुविधाएं और अधिक विविध सहकर्मी समूह प्रदान करते हैं, जिससे सीखने का अनुभव बढ़ता है। समेकन, शिक्षक तैनाती को तर्कसंगत बनाने, बेहतर शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने में मदद करता है। कम लेकिन बड़े स्कूलों के साथ, शासन और निगरानी अधिक प्रभावी हो जाती है, बेहतर शासन से स्कूल का प्रदर्शन बेहतर होता है और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आती है, जैसा कि स्कूल विलय के परिणामों में देखा गया है। जैसा कि साथ- ई परियोजना में देखा गया है।
स्कूल विलय में वस्तुतः निम्न विचार ध्यान में रखना चाहिए जैसे पहुंच सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए कि छात्र बिना किसी कठिनाई के बड़े, विलय किए गए स्कूलों में जा सकें। दूर-दराज के इलाकों के छात्रों के लिए बसों की व्यवस्था करने के लिए मानक आदर्श खूंटी जिले के दृष्टिकोण का अनुकरण किया जा सकता है। शिक्षक युक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए, सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए विलय किए गए स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। नजदीकी स्कूलों को बनाए रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए, दूर स्थित स्कूली शिक्षा के कारण स्कूल छोड़ने की बढ़ती दर को रोकने के लिए। स्कूल विलय से कुछ चिंताएं उपजती हैं ,जैसे शिक्षा तक पहुंच, स्कूलों के विलय से यात्रा की दूरी बढ़ सकती है, जिससे संभवतः स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है, खासकर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुपालन, कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विलय आरटीई अधिनियम का उल्लंघन कर सकता है, जो पड़ोस के स्कूलों में शिक्षा की गारंटी देता है। कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि स्कूलों को बंद करना या विलय करना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 3 और 8 का उल्लंघन है। धारा 3 छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 8 उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य सौंपती है कि वह प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। इनमें से अधिकांश स्कूल पहाड़ी इलाकों के आदिवासी इलाकों में हैं। किसी गाँव में स्कूल बंद होने से ड्रॉपआउट दर में ही वृद्धि होगी क्योंकि छात्रों के लिए स्कूल जाने के लिए दूर तक यात्रा करना संभव नहीं होगा। अभिभावकों को यह भी चिंता सताती रही है कि अगर उनके बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे तो वे मध्याह्न भोजन से भी वंचित हो जायेंगे। साथ ही भारत जैसे विशाल देश में सांस्कृतिक और भौगोलिक चुनौतियाँ होना भी लाजमी है, भारत जैसे विविध राज्यों में, स्कूल विलय का एक आकार-सभी के लिए एक दृष्टिकोण सभी समुदायों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
शिक्षा हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है और उसे यह अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जिस उतावलेपन के साथ सरकारी स्कूल बंद किए गए और बंद किए जा रहे हैं, क्या उसे देखकर लगता है कि बच्चों को उनका निशुल्क शिक्षा का अधिकार छीनने की गुपचुप कहीं तैयारी तो नहीं चल रही है?
शिक्षा हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है और उसे यह अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जिस उतावलेपन के साथ सरकारी स्कूल बंद किए गए और बंद किए जा रहे हैं, क्या उसे देखकर लगता है कि बच्चों को उनका निशुल्क शिक्षा का अधिकार छीनने की गुपचुप कहीं तैयारी तो नहीं चल रही है? जरा सोचिए कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से देश में करीब 2 लाख सरकारी स्कूल खस्ताहाल और अनुपयोगी बताकर बंद कर दिए गए हैं, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो दूर गांवों में बसे वो बच्चे, जिन्हें पगडंडियों से होकर बाहर आने में ही घंटों लग जाते हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा? जब सरकारें खुद खस्ताहाल स्कूलों को सुधारने का काम नहीं करेंगी, तो स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट ( बीच में विद्यालय छोड़ने की दर) कैसे कम होगी? कहीं सरकारी स्कूल बंद करना खुद शिक्षा की जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेने और बच्चों को निजी स्कूलों तक पहुंचने के लिए मजबूर करने की कोई साजिश तो नहीं है? वैसे भी नीति आयोग ने 2017 में स्कूल विलय नीति का मसौदा तैयार कर कर लागू किया था 2020 तक की अवधि में स्कूल विलय नीति का कार्यकाल खत्म होना था लेकिन अभी 2023 में भी महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश की सरकारों ने 20 से कम छात्रों के नामांकन वाले कई स्कूलों को विलय करके स्कूलों के समूह बनाने की एक नई योजना को मंजूरी दे दी है।16 राज्यों ने नीति आयोग के प्रोजेक्ट (प्रयोजना) प्रस्तावना पर प्रतिक्रिया दी थी, और 14 राज्यों के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया था।
रपट के मुताबिक, अंततः झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश को इसके लिए चुना गया था। हाल ही की रपट देश भर में सार्वजनिक स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में अब तक सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए इन तीन राज्यों में देखे गए परिणाम पर आधारित है और इन तीन राज्यों के स्कूल विलय नीति के परिणाम सुखद रहे हैं।स्कूल शिक्षा में 4 साल में 12 रैंक ऊपर आया मध्य प्रदेश। स्कूल विलय नीति प्रोजेक्ट के तहत एक किमी के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश के 35 हजार स्कूलों का 16 हजार स्कूलों में विलय कर दिया गया। नतीजतन 55 फीसदी स्कूलों में प्राचार्य /प्रधानाध्यापक की कमी दूर हो गई। स्कूल शिक्षा में मध्यप्रदेश 2017 में 17 वें पायदान पर था। अब पांचवें पायदान पर है। चार साल में प्रदेश ने 12 पायदान की छलांग लगाई। यह सबकुछ एक शाला-एक परिसर के तहत हुआ। शाला दर्शन के तहत अफसरों से स्कूलों के आधारभूत ढांचा गत संरचना और शिक्षा की मॉनीटरिंग कराई। स्कूल से फोटो भेजना अनिवार्य किया गया। जिसका असर भी दिखा। वहींओडिशा सरकार ने 15 जिलों में लगभग 8,000 स्कूलों की पहचान की और कम नामांकन (20 से कम छात्र) की वजह से अन्य स्कूलों में विलय करने का वायदा किया गया और तकरीबन 2000 से अधिक विद्यालय विलय किए गए और इसे बड़ी चालाकी से स्कूलों का एकीकरण और युक्तिकरण कहा गया है। झारखंड में भी स्कूल विलय नीति के तहत 4380 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए।
यह सच है कि विलय से स्कूल छात्रों के लिए आकांक्षी बनेंगे और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार होगा। अतिरिक्त ई-लर्निंग और सह-पाठयक्रम सुविधाओं के साथ बेहतर बुनियादी सुविधाएं, बेहतर शैक्षणिक माहौल होगा। हालाँकि, स्कूलों को बंद/विलय करने से पहले भौगोलिक बाधाओं और अन्य बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया को संचार के स्पष्ट माध्यमों, एक कठोर शिकायत निवारण प्रणाली और संपूर्ण परामर्श के माध्यम से सक्षम किया जाना चाहिए।


Pingback: हरित इस्पात पर्यावरण के बेहद अनुकूल - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: वसंत पंचमी महापर्व - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: मध्य प्रदेश की जीवन रेखा सदानीरा माँ नर्मदा - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान: एक महत्वपूर्ण कदम - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: घातक महामारी बनता क्षयरोग - Jan Abhyuday Kranti News
Pingback: दुनिया के 60 फीसद कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए सिर्फ 12 देश जिम्मेदार - Jan Abhyuday Kranti News